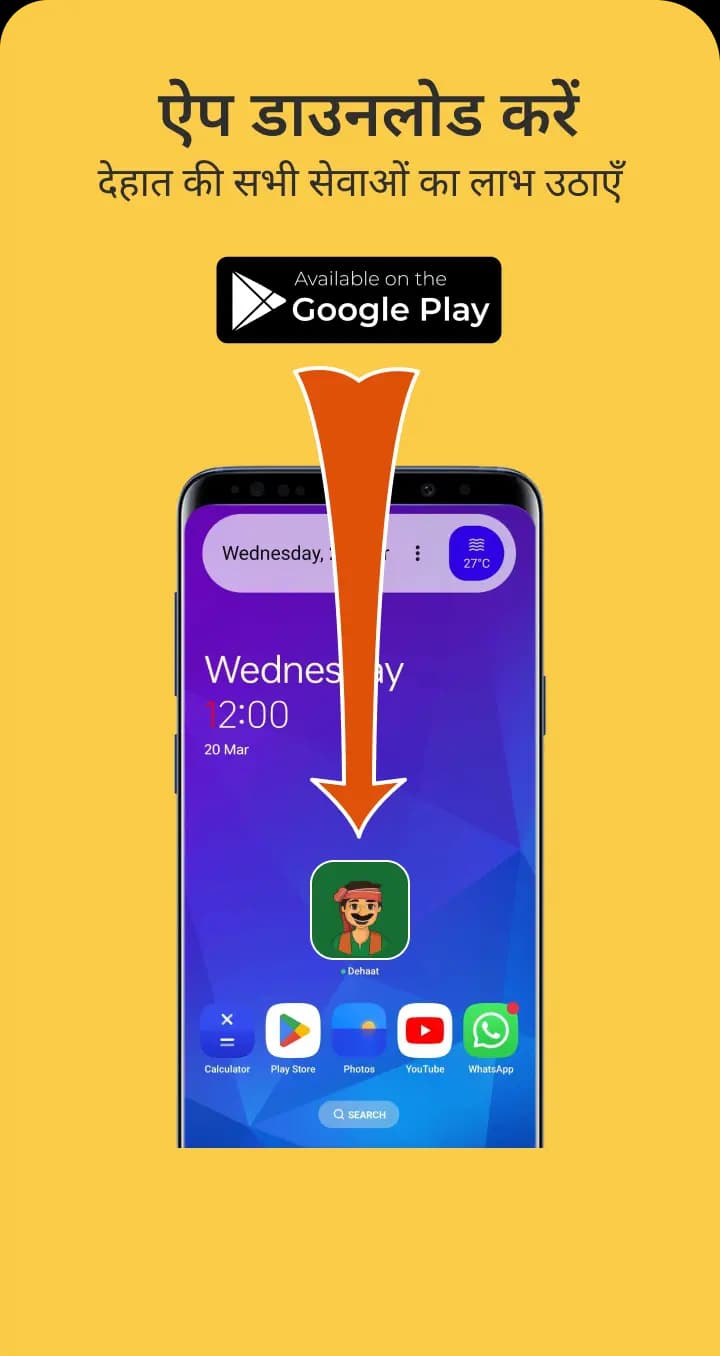मृदा परीक्षण के फायदे एवं नमूना लेने की विधि | Soil Testing: Advantages and Sampling Process

मृदा परीक्षण के फायदे एवं नमूना लेने की विधि | Soil Testing: Advantages and Sampling Process
मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है जो फसलों की पैदावार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मिट्टी में कई तरह के पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं जैविक पदार्थ मौजूद होते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बलुई मिट्टी, भारी मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, आदि कई तरह की मिट्टी पाई जाती है। सभी की अपनी विशेषता, अपनी अलग भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए लाभदायक है। खेत में लम्बे समय तक हानिकारक रासायनिक पदार्थों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है और फसल की पैदावार और गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई वर्षों के अनुभव के बाद भी किसानों के लिए मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का अंदाजा लगाना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में फसलों की पैदावार पर प्रभाव पड़ता है। उच्च गुणवत्ता की फसल और अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए मिट्टी में मौजूद तत्वों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ऐसे में मिट्टी की जांच इस समस्या से बचने का एक बेहतर विकल्प है। मृदा परीक्षण यानि मिट्टी की जांच करा कर किसान इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मिट्टी जांच के क्या हैं फायदे? | Benefits of Soil Testing
- मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार: मृदा परीक्षण से किसानों को मिट्टी का पीएच स्तर और उसमे मौजूद जैविक तत्वों, लवणों, पोषक तत्वों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की सटीक जानकारी मिलती है। इससे जिन पोषक तत्वों की कमी है उनकी पूर्ति करके मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।
- मिट्टी की उर्वरक क्षमता: मिट्टी जांच से इसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाने में आसानी होती है।
- फसल की उपज एवं गुणवत्ता: उचित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग करने से फसलों की उपज एवं गुणवत्ता दोनों बेहतर होती है।
- पौधों का बेहतर स्वास्थ्य: मृदा परीक्षण से किसानों को मिट्टी से होने वाली बीमारियों और कीटों की पहचान करने में मदद मिलती है, जिससे फसलों को क्षति पहुंचने से पहले इन पर नियंत्रण किया जा सकता है।
- पर्यावरण संरक्षण: मृदा परीक्षण किसानों को उर्वरकों और अन्य रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से बचने में मदद करता है, जिससे मिट्टी और जल प्रदूषण में कमी आती है।
- अधिक मुनाफा: मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों के अनुसार फसलों का चयन कर अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। जिससे किसानों को अधिक मुनाफा प्राप्त होता है।
मिट्टी जांच कब करानी चाहिए? | When to do Soil Testing?
- बेहतर फसल प्राप्त करने के लिए फसल की बुवाई या रोपाई से एक महीना पहले खेत की मिट्टी की जांच कराएं।
- अगर आप सघन पद्धति से खेती करते हैं तो हर वर्ष मिट्टी की जांच करवानी चाहिए।
- यदि खेत में वर्ष में केवल एक फसल की खेती की जाती है तो हर 2 या 3 वर्षों के अंतराल पर मिट्टी की जांच करना जरूरी है।
मिट्टी जांच कहां से कराएं? | Where can you get Soil Testing done?
- मिट्टी जांच करने के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग या कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
- इसके अलावा आप 'देहात' के द्वारा भी मिट्टी की जांच करा सकते हैं।
- इसके लिए आपको यहां दिए गए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरना होगा।
- फॉर्म में आपके द्वारा चयनित समय पर देहात एग्जीक्यूटिव मिट्टी का नमूना लेंगे।
- भुगतान के 7 दिनों के अंदर आप मिट्टी जांच का रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
मिट्टी जांच के लिए नमूना लेने की विधि | Procedure for Soil Sampling
- जिस खेत की मिट्टी की जांच करवानी है उस खेत में 8-10 जगह निशान लगा लें।
- निशान लगाए सभी जगहों से घास, कंकड़, पत्थर आदि हटा दें।
- सभी स्थानों में 15 सेंटीमीटर गहराई तक खोद कर मिट्टी निकालें।
- अब सभी गड्ढों से 2-3 सेंटीमीटर मिट्टी निकालें। सभी गड्ढों से निकाली गई मिट्टी को अच्छी तरह मिला दें।
- अब मिट्टी को चार भागों में बांट लें। आमने-सामने के दो भागों की मिट्टी को मिला दें और शेष मिट्टी फेंक दें।
- मिट्टी के करीब 500 ग्राम होने तक इस प्रक्रिया को दुहराएं। इस तरह से लिया गया नमूना पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
- इस नमूने के साथ अपना नाम, पूरा पता, खेत की पहचान, नमूना लेने की तारीख, जमीन की ढलान, सिंचाई का स्त्रोत, जल निकासी, अगली बुवाई करने की फसल, पिछले वर्ष की फसलों की जानकारी आदि विवरण के साथ जांच के लिए कृषि विकास प्रयोगशाला में भेज दें।
मिट्टी का नमूना लेने के समय रखें इन बातों का ध्यान | Things to Keep in Mind While Collecting Soil Samples
- गीली मिट्टी का नमूना न लें। अगर मिट्टी गीली है तो मिट्टी के नमूने को छांव में सूखाने के बाद जांच के लिए भेजें।
- मिट्टी के नमूने को दूषित होने से बचाने के लिए किसी साफ थैली का प्रयोग करें।
- अगर एक ही खेत के विभिन्न स्थानों में अलग-अलग फसलों की खेती की जाती है तो उनका नमूना भी अलग अलग ही लें।
- जिस खेत में हाल ही में कम्पोस्ट खाद, अन्य जैविक या रासायनिक खाद, चूना, जिप्सम आदि का प्रयोग किया गया है उस खेत की मिट्टी का नमूना न लें।
- खेत की मेड़ें या रास्तों की मिट्टी का नमूना नहीं लेना चाहिए, खेत के किनारों से कम से कम 1-1.5 मीटर अंदर की तरफ से नमूना लें।
नोट:
- 'देहात' के द्वारा मिट्टी की जांच के लिए यहां क्लिक करें।
- देहात के द्वारा मिट्टी जांच की सुविधा अभी केवल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं हरियाणा में उपलब्ध है। आने वाले समय में भतार के अन्य राज्यों में भी इस सुविधा की शुरुआत की जाएगी।
क्या आपने कभी अपनी खेत की मिट्टी की जांच कराई है? अगर हां, तो इससे आपको कितना लाभ मिला है? अपने जवाब एवं अनुभव आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। कृषि में आधुनिक तकनीकों की अधिक जानकारी के लिए 'कृषि टेक' चैनल को अभी फॉलो करें। इस जानकारी को अधिक किसानों के साथ साझा करने के लिए इस पोस्ट को लाइक और शेयर करना न भूलें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | Frequently Asked Question (FAQs)
Q: मिट्टी की जांच कैसे की जाती है?
A: खेत के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी के नमूनों को एकत्र करके अपने नजदीकी कृषि विभाग या कृषि विश्वविद्यालय भेजें। इसके बाद वहां प्रयोगशाला में मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण करके उसका परीक्षण किया जाता है। जांच होने के बाद आपको इसकी रिपोर्ट भेज दी जाती है।
Q: मिट्टी परीक्षण कब करना चाहिए?
A: किसी भी फसल को लगाने से पहले या हर तीन वर्ष में कम से कम एक बार मिट्टी की जांच कराना जरूरी है। भारत में, मिट्टी परीक्षण करने के लिए वर्षा का मौसम शुरू होने से पहले यानी मार्च से जून या वर्षा का मौसम समाप्त होने के बाद यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय उपयुक्त माना जाता है।
Q: मृदा परीक्षण क्यों करवाना चाहिए?
A: खेत की जुताई एवं मिट्टी में होने प्रयोग किए जाने वाले हानिकारक रसायनों के कारण मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होने लगती है। जिससे धीरे-धीरे फसलों की उपज कम होने लगती है। मिट्टी जांच से मुख्य तत्वों जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्सिशयम, मैग्नीशियम और सूक्ष्म तत्वों जैसे जस्ता, मैग्नीज, तांबा, लौह, बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन की मात्रा और पीएच स्तर की जानकारी मिलती है। जिनमें सुधार करते हुए हम फसलों की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं।
जारी रखने के लिए कृपया लॉगिन करें

फसल चिकित्सक से मुफ़्त सलाह पाएँ